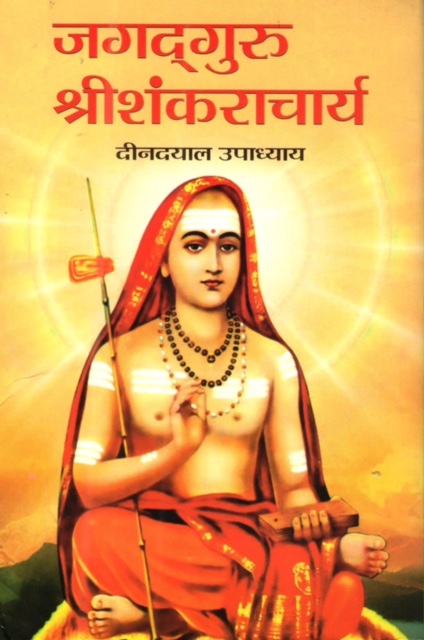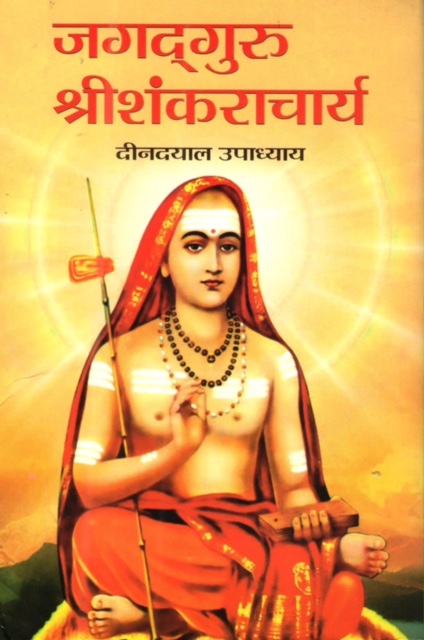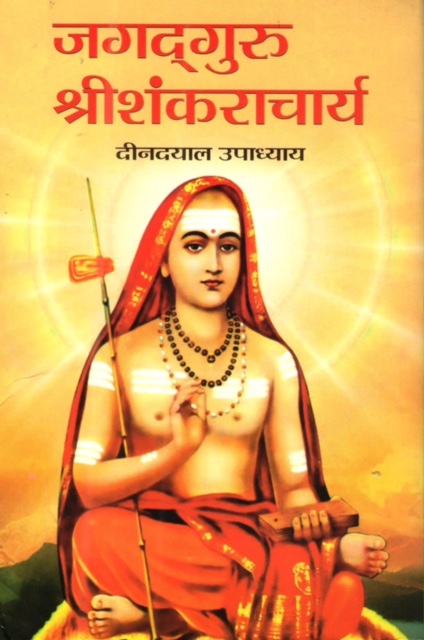
दीनदयाल जी द्वारा लिखित श्री जगद्गुरू शंकराचार्य जी
पुस्तक समीक्षा
एकात्म मानववाद प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महान औपन्यासिक कृति ‘जगद्गुरू शंकराचार्य’ -डाॅ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृति हमारी सामाजिक अंतःक्रियाओं का आधार है। ज्ञान-विज्ञान, कलाएं तथा जीवन से जुड़ा हमारा तमाम आचार-व्यवहार संस्कृति से ही तो निबद्ध है। जगद्गुरू शंकाराचार्य ने विविधताओं में गुंथी इसी भारतीय संस्कृति को एक समय में विलुप्त होने से बचाने और इसमें व्याप्त रूढ़ियों से मुक्त कर इसकी सनातनता को स्थापित किया। भारतीय संस्कृति, दर्शन और ज्ञान-विज्ञान के उदात्त मूल्यों के उन्नायक रूप में जगद्गुरू शंकराचार्य ने जो किया वह अपूर्व है। यह वही शंकराचार्य हैं जो 8 वर्ष की अल्पायु में चारों वेदों में निष्णात हो गए थे, 11 वर्ष की आयु में शास्त्रों में पारंगत हो गए और 32 वर्ष की अल्पायु तक में जिन्होंने ईष, केन, प्रष्न, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छान्दोग्योपनिष्द् पर भाष्यों की रचना कर, संपूर्ण भारत का भ्रमण कर विश्व को समन्वय का पाठ पढ़ा दिया था। आदि शंकाराचार्य ने देश को एकता के सूत्र में ही नहीं बांधा बल्कि सनातन भारत की संस्कृति को विश्व भर में प्रतिस्थापित किया। बौद्ध धर्म की व्याप्ति में एक समय में भारत से समाप्तप्राय होते जा रहे हिंदू धर्म को फिर से जीवित करके उन्होंने सनातन भारतीय संस्कृति की जड़ों को हरा किया।
एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सद्य प्रकाशित औपन्यासिक कृति ‘जगद्गुरू शंकराचार्य’ को पढ़ते समय आदि शंकराचार्य के इस जीवन मर्म में ही जैसे पाठक प्रवेश करता है। शंकाराचार्य पर बहुत कुछ पहले भी लिखा गया है परन्तु दीनदयाल उपाध्याय की यह कृति इस मायने में विरल है कि इसमें उनके महामानव की बजाय एक साधारण मानव रूप में कथा के ताने-बाने को बुनते सनातन राष्ट्र की उनकी संकल्पना के लिए किए कार्यों को उद्घाटित किया गया है।
जगद्गुरू शंकराचार्य का संपूर्ण जीवन ही अपने आप में संदेश है। मुझे लगता है, वह पहले ऐसे संन्यासी हैं जिन्होंने जड़ होते जीवन मूल्यों पर प्रहार करते विश्व को अद्वैत का दर्शन ही नहीं दिया बल्कि बंधे-बंधाए नियमों और निर्धारित रूढ़ियों के जड़त्व को तोड़ा। उनके जीवन दर्शन से साक्षात् कराती यह कृति उनके अवतरण, बाल्यकाल के साथ ही उनकी दिग्विजय यात्रा, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ, भारती का समाधान, हिमालय की चोटियों पर और महत्व में विलीन जैसे शीर्षकों से रोचक आख्यान प्रस्तुत करती हैं।
महत्ती यह भी है कि सहज परन्तु सधे शब्दों में शंकराचार्य से जुड़े जीवन प्रसंगों के साथ ही उपाध्याय जी की यह कृति उनके दर्शन के गूढ़ रहस्यों को सहज-सरल रूप में संप्रेष्य करती है। कथा कहने का उनका अंदाज कुछ ऐसा है कि पाठक उसके प्रवाह में स्वयमेव बहता चला जाता है। शंकराचार्य के चरित्र चित्रण की उनकी व्यंजना मन को गहरे से मथती है। संन्यास ग्रहण कर गुरू की खोज में निकले क्षणों का शब्द चित्रण देखें, ‘अंतःकरण की धनाढ्यता ही उनका एकमात्र धन था। आत्मविश्वास की प्रबलता ही उनकी महती शक्ति थी। प्रगल्भ बुद्धि ही उनका पथ-प्रदर्शन कर रही थी। हृदय में अपने कार्य पर असीम श्रद्धा तथा भगवान का एकमात्र सहारा ही उनका बल था। वे बड़ी शांति तथा अपने अंदर एक प्रकार की चैतन्य शक्ति का अनुभव कर रहे थे, यही उनहें स्फूर्ति प्रदान कर रही थी।…उसी समय उन्होंने ‘अच्युताष्टक’ नाम की भक्ति भाव से परिपूर्ण कविता की रचना की।’
दीनदयाल उपाध्याय की इस कृति की बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें कथा के ताने-बाने में जगद्गुरू शंकाराचार्य के दर्शन को ठौड़-ठौड़ उद्घाटित किया गया है। संन्यास लेने के बाद शंकर की भेंट अपने सहपाठी विष्णु शर्मा से होती है। विष्णु जब उनसे संन्यास के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने का प्रश्न पूछता है तो उनका जवाब होता है, ‘संन्यास का अर्थ संसार को छोड़कर वन में तपस्या करना नहीं है। मैंने कर्म संन्यास लिया है, जिसका अर्थ कर्म से भागना नहीं, देश और धर्म के कर्म करना है, जो सत्य है तथा मनुष्य को कर्मफल-बंधन में नहीं बांधते।’
उपन्यासकार दीनदयाल उपाध्याय का यह एक वाक्य ही इस औपन्यासिक कृति का जैसे सार है। उन्होंने इसमें शंकराचार्य के ‘कर्म संन्यास’ के बहाने राष्ट्र के और मानव मात्र के लिए किए उनके अद्भुत कार्यों के उजास में धर्म और धर्माचार्य की भारतीय सनातन परम्परा को जैसे गहरे से जिया है। उपन्यास पढ़ते संन्यास जीवन के मर्म में हम प्रवेश करने जैसे जीवनगत सरोकारों की शंकर के ओज से भी नहा उठते हैं। यह सच है, शंकर ने जो किया वह अद्भुत और अपूर्व था। इसलिए भी कि वह परम्परागत संन्यास के बंधे-बंधाए ढर्रों को बारम्बार तोड़ते हैं। एक स्थान पर उपन्यास में शंकाराचार्य कहते भी हैं, ‘अपने बनाए हुए नियमों के हम स्वामी हैं, दास नहीं।’ लकीर पीटने की बजाय उन्होंने समाज को कर्म करते लक्ष्य प्राप्ति का ही तो संदेदिया था। इसीलिए उपन्यास में वह कहते भी हैं, ‘व्यवस्था और नियम साध्य नहीं, साधन है। साधन का उपयेाग तब तक है, जब तक वह साध्य को प्राप्त करने में सहायक हो। केवल लकीर पीटने से क्या लाभ?’
दीनदयाल उपाध्याय के पास कहन का अनूठा अंदाज है। इस अंदाज में उपन्यास की उनकी कथा में वैदिक धर्म के तीन तत्व ज्ञान कणादि के वैषेषिक दर्शन, गौतम के न्याय दर्शन और कपिल के सांख्य दर्शन से भी पाठक रू-ब-रू होते हैं तो अवैदिक मतावलंबियों के चार्वाक के लोकायत दर्शन, जैनों के अर्हत् तथा बौद्धों के तथागत दर्शन से भी साक्षात् होते हैं। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इस कृति में शंकाराचार्य के जीवन दर्शन के बहाने दीनदयाल उपाध्याय जी ने तत्कालीन ज्ञान और दर्शन को भी गहरे से रेखांकित किया है। बौद्ध संस्कारों के वर्चस्व के दौर में हिंदू धर्म की जड़ों को सींचने, काशी में रहते भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए कार्य करने, हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के सनातन स्त्रोत और उसके अजस्त्र प्रवाह के अवरोधेां को दूर करने के लिए शंकराचार्य द्वारा अपनाई गई युक्तियों के साथ ही राष्ट्र की संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करने संपूर्ण भारत के उनके भ्रमण की रोचक दास्तां ‘जगद्गुरू शंकराचार्य’ कृति है।
इस कृति की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भारतीय संस्कृति की वैदिक परम्परा और अवैदिक परम्परा के साथ ही वैदिक, अवैदिक दर्शनों पर गंभीर चिंतन को सहज कथा में गूंथा गया है। शंकर के जीवन की इस विशेषता को भी यह उपन्यास गहरे से उद्घाटित करती है कि बंधन से मुक्ति ही असल संन्यास है। लोग घरों से बाहर निकलें और सनातन भारत से भेंट करें, इसीलिए शंकराचार्य ने देश के चार अलग-अलग कोनों में पीठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रिकाश्रम, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में जगन्नाथ पीठ की स्थापना के पीछे आदि शंकराचार्य की यही तो मंशा थी कि अपने खोल से बाहर निकल व्यक्ति जीवन की उदात्ता के दर्शन करें। सनातन भारतीय संस्कृति से रू-ब-रू हों। धर्म यात्रा के दौरान ही शंकराचार्य को अपनी माता की बीमारी का पता चलता है। माता ने उनके लिए अंतिम समय में संजोया कुछ धन भेजा है। शंकाराचार्य माता का समाचार पाकर बहुत व्यथित होते हैं। धन का उनके लिए क्या उपयोग! यह संपति उनकी नहीं राष्ट्र की है। उन्होंने माता के भेजे धन से बद्रिकाश्रम में बदरीनाथ का मंदिर बना दिया।
संन्यास लेने के बाद कोई फिर से घर नहीं लौटता। पर शंकराचार्य आम संन्यासी नहीं थे। उन्होंने निरंतर उन नियमों को तोड़ा जो जीवन के कर्म पथ के बाधक थे। माता से उन्होंने वादा किया था कि अंतिम समय में उनके पास रहूंगा। सो वह बद्रिकाश्रम से मां के पास कालटी पहुंचे। उनके स्नान के लिए पूर्णा नदी को ही घर ले आए। मां के आग्रह पर उन्हें अद्वैत दर्शन समझाने तत्वबोध ग्रंथ रचा। पर मां ने जब कृष्ण के विषय में कुछ बताने को कहा तो उनके लिए ‘कृष्णाष्टक’ बनाकर उन्हें सुनाया। संन्यासी को दाहकर्म की आज्ञा नहीं होती परन्तु शंकराचार्य सच्चे संन्यासी थे। केवल कपड़े रंगकर दिखावा करने वाले नहीं। कुटुम्ब के लोगों ने संन्यासी होते हुए फिर से घर लौटने के कारण उनका बहिष्कार कर दिया था। मां की चिता को कौन अग्नि दे। मां के लिए शंकर ने इस नियम को भी तोड़ा। उन्होंने अपने घर के आंगन में ही मां की चिता रचकर उनका अग्नि संस्कार किया। अभी दाह संस्कार किया ही था कि गुरू गोविंदपाद के रूग्ण होने का संदेश मिला। वे कालटी से अमरेष्वर के लिए रवाना हो गए। एक माह में वहां पहुंचे। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष और यात्राओं से भरा था परन्तु उन्होंने कर्म को ही अपने जीवन का संदेश बनाते संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति के लिए कार्य किया।
शंकराचार्य ऐसे संन्यासी थे जिन्होंने अपने शिष्यों की भी सेवा की। उदंक को कुष्ठ रोग से मुक्त किया। हस्तामलक को विक्षुब्ध अवस्था से बाहर निकाला। चांडाल को उन्होंने अपना गुरू माना। मनीषपंचक नाम विख्यात पांच श्लोंकों की रचना की। ऐसे जगद्गुरू शंकाराचार्य के विराट जीवन और दर्शन को कथा के ताने-बाने में बुनना आसान नहीं है परन्तु दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने इस उपन्चयास ‘जगद्गुरू शंकाराचार्य’ में जैसे गागार में सागर भरा है। उनके जीवन के छोटे से छोटे प्रसंग और उससे जुड़े दर्शन को व्याख्यायित करते उन्होंने जैसे सनातन भारतीय संस्कृति के उस उन्नायक का चित्र हमारे समक्ष उद्घाटित किया है। इसमें शंकराचार्य से जुड़े कथानक को सामान्य मानव रूप में उद्घाटित किया गया है। यह नहीं कि चमत्कारिक रूप में उन्हें ईश्वरीय स्वरूप प्रदान किया गया है।
यह है तभी तो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ में शंकराचार्य ने इस कृति में बाह्य यज्ञ के स्थान पर आत्मयज्ञ पर जोर दिया। उन्होंने भक्ति की सनातन प्रेरणा और उसी के विकसित रूप में जनसाधारण की पूजा पद्धति आदि के साथ ही जो कुछ मनुष्य जीवन के उपभोग के लिए नहीं बल्कि मानव आदर्शों की प्राप्ति के लिए करते हैं, उसे ही यज्ञीय भावना बताया। मंडन मिश्र की पत्नी भारती द्वारा अपने पति की हार को देखते शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने और गृहस्थ आश्रम से जुड़े प्रश्न पूछने के दौरान भी दीनदयाल जी ने शंकराचार्य द्वारा छः माह का समय मांगने और इस दौरान मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने को किवदंती बताते सांसारिक ज्ञान प्राप्ति की बात कही है। ऐसे ही बहुतेरे दूसरे प्रसंगो में भी दीनदयाल जी ने शंकराचार्य के जीवन की विशेषताओं में ही उनके कर्म संदेश को संप्रेषित किया है।
सनातन भारतीय संस्कृति के पुरोधा जगद्गुरू शंकाराचार्य का दर्शन सगुण ब्रह्म के साथ ही निर्गुण ब्रह्म से भी जुड़ा है। उनके लिखे भाष्यों के साथ ही नर्मदाष्टकम् और दूसरी कृतियों के पारायण के पीछे भी रही मानव कल्याण की भावना, उनके दृढव्रत जीवन के साथ ही राष्ट्र जीवन की रचना के उनके कार्यों का यह उपन्यास जैसे सार है। भारत की आंतरिक एकता के लिए किए शंकराचार्य के किए गए प्रयासों के साथ सबके कल्याण के उनके संदेश का यह उपन्यास जैसे मनोरम कथा कोलाज है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निबंधात्मक लेखन से तो पाठक पहले से परिचित हैं परन्तु ‘जगद्गुरू शंकाराचार्य’ के बहाने उनके कथाकार स्वरूप से भी साक्षात् हुआ जा सकता है। यह कृति कोई सात दशक पहले उन्होंने लिखी थी परन्तु इधर यह अप्राप्य थी। उपाध्याय जी के चिंतन के साथ ही उनके कथाकार से रू-ब-रू कराती यह कृति शब्दों की उज्ज्वल दीठ है।
Post Views: 1,962